शोध-आलेख
विद्यापति के काव्य में स्वरों की
संगीतमयता
- डॉ.
सूर्यकान्त त्रिपाठी
संगीत
स्वयं आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है। संगीत में ही वह शक्ति है कि आराधक अपने आराध्य
को सहज ही वश में कर लेता है क्योंकि स्वभावतः संगीत की धारा मधुर होती है,
वह जीवन की शंकुल परिस्थितियों में दिव्य ज्योति का भी दर्शन कराती
है और निष्क्रिय जीवन में सक्रियता का अमित उत्साह भर देती है। हम अपने काव्य की
छंद शैलियों का वैविध्य जब देखते हैं तो संगीत-रुचि के नवनवोन्मेषशालिनी शक्ति का
ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भावों में आकर्षण की सहज रमणीयता संगीत के द्वारा
ही सम्पन्न होती है। यही कारण है कि हिन्दी के आदि कवि के काव्य का आरम्भ प्रकृति
की सहज संगीत माधुरी के स्वर में प्रस्फुटित हुआ है। चण्डिदास, विद्यापति, गोविन्ददास, सूरदास
आदि ने काव्य की संगीतमयी साधना से ही अमृततत्व का प्रत्यक्ष किया है। कविवर
विद्यापति की गीतमयता काव्य की अपूर्व चत्मकृति से मिलकर चैतन्य महाप्रभु जैसे
साधक को भी वशीभूत करने में समर्थ हुई है।
इस
प्रकार कवि विद्यापति के काव्य में अनंत चमत्कृतियों के साथ स्वरों की संगीतमयता
ही भाषा में सप्राण आकर्षण का आधार बनी हुई है। विद्यापति में एक ओर युग-जीवन के
निसर्ग सौंदर्य-प्रवाह की रसप्लाविनी झंकृति प्राप्त होती है तो दूसरी ओर दृश्यविधायिनी
चमत्कृति का अपूर्व दर्शन भी प्राप्त होता है। काव्य और संगीत की सर्वरंजनकारिणी
समन्विति का जो प्रकाश-वितरण इस अमर गायक ने किया है। उससे यौवन के चरममाधुर्य और
वार्धक्य के चरम गांभीर्य की जीवनव्यापिनी श्रुति प्राप्त होती है। संगीत की
तरंगों की तन्मयतापूर्ण समाधि में नारी की रूप माधुरी का अनुपम प्रत्यक्ष है।
भावुकता और कल्पना का अद्भुत समन्वय निम्नवत् देखा जा सकता है-
चाँद-सार
लए मुख घटना करूँ,
लोचन
चकित चकोरे ।
अमिय
धोय ऑचर धनि पोछलि,
दह
दिपि भेल उँजोरे । 1
एक ओर पुरुष
हृदय की तरल अतृप्ति का चिरन्तन भावावेश संगीत की मादक लहरों में अद्भुत मोहकता के
साथ इस रूप में श्रवणगत होता है-
सजनि,
भल कए पेखल न भेल।
मेघ
माल सयॅ तडि़तलता जनि,
हृदय
सेल दइल गेल।
दूसरी ओर
नारी-सृष्टि की अनन्य आत्मीयता की उपलब्धि का निश्छल अनुराग भी सुनाई देता है-
की लागि कौतुक
देखलौ सखि,
निमिख
लोचन आध।
मोर
मन-मृग मरम बेघल,
विषम
बान बेआध।
भावना के
चरम-दिव्य भावावेश को तरंगायित करने में विद्यापति की कला द्रुत-हृदयस्पर्शिनी
हैः-
विपत
अपत तरू पाओल रे,
पुन
नव-नव पात।
बिरहिन-नयन
बिहल बिहि रे।
अविरल
बरिसात। 2
लोकगीतों
में नारी की विरह वेदना का जितना सजीव चित्र उरेहने में कवि विद्यापति को कामयाबी
मिली है, कदाचित् हिन्दी वांगमय में अन्य कवियों को उतनी
नहीं। विरहानुभूति की मार्मिकता का सजीव चित्र प्रकृति के माध्यम से इसे रससिद्ध
कवि ने इस प्रकार खींचा है, मानों नारी हृदय का सार एकत्र हो गया
है। प्रकृति के मोहक समय में विरहिणी की अंर्तव्यथा उसके हृदय की वीणा में इस
प्रकार झनझना उठती है-
के
पतिआ लए जायत रे,
मोरा
पियतम पास।
हिए
न हि सहए असए दुखरे,
भेल
साओन मास।
एक
सरि भवन पिया बिनु रे,
मोरा
रहलो न जाय।
सखि
अनकर दुख दारून रे,
जग
से पतिआय। 3
नारी हृदय का
सनातन अनुराग ही अपने चरम भावावेष में पिघलकर जैसे प्रवाहित हो रहा है। ग्राम्य
संस्कृति की अनुरूपता के साथ पौराणिक विश्वास की अनुवर्तिता वे गायक स्वरों में
रस-पेशलता के साथ दिव्य भावोन्माद की अपूर्वता का अमृतमय आकर्षण भर दिया है-
मधुपुर
मोहन गेल रे
मोरा
विहरत जाती।
गोपी
सकल बिसरलनि रे
जत
छल अहिबाती।
’ ’ ’
कत
कहबो कत सुमिरब रे,
हम
भरिए गरानि।
आन
कऽ धन सो धनवन्ती रे,
कुबजा
भेल रानि। 4
विरह प्रधान
गीतों में उपालम्भ की मर्मस्पर्शिता निसर्गतः बेधिनी है, विरहिणी
की करूणा अनन्याशक्ति की माधुरी में द्रवित हो रही है-
सब
करि पहु परदेस बसि सजनी,
आयल
सुमिरि सिनेह।
हमर
एहन पति निर्दय सजनी,
नहीं
मन बाढ़य नेह। 5
विद्यापति ने
राधा को भारतीय नारी की विरहासक्ति की चरम प्रकाश के रूप में चित्रित किया है,
वस्तुतः राधा आराध्या है। संगीत की स्वरलहनी में रमणी की दिव्य भावना
मूर्ति परम रमणीय हो गयी है-
माधव,
देखलि वियोगिनी वामे,
अधर
न हास विलास सखि संग,
अहोनिसि
जप नू नामे। 6
गीतिकार कवि की
कला की पूर्ण संगीतमयता की प्रतीति विविध वाद्यों की अनुरणन-ध्वनि की अनुकृति से
भलीभाँति हो जाती है, रसलीला की इस दृष्यानुभूति में गीत,
वाद्य और नृत्य की अपूर्व झंकृति सुनाई दे रही है-
बाजत
द्रिगि-द्रिगि धौ द्रिम-द्रिमिया।
नटति
कलावति माति ष्याम संग,
कर
करताल प्रबंधक ध्वनियाँ।
डम-डम
डंक डिमिक डिम मादल,
रुनु
झुनु मंजीर बोल।6
वाद्य ध्वनि की
रसमयी प्रतीति बहुषः गीतों की सुखद-श्रुति से सहज ही मिल जाती है। नाद-सौंदर्य की
सजीवता ही संगीत का प्राण है, इसका प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत गीतांश से
पूर्णतया स्पष्ट है-
रंगिनी
गन सब रमिहि नटई
रन
रनि कंकन किंकिन रटई,
रहि
रहि राग रचय रसवन्त।
रति
रत रागिनी रमन बसन्त।।
गीतिकार कवि का
सबसे बड़ा वैशिष्टय यह है कि उसने लौकिक प्रेम भावना को सौंदर्य की माधुर्यानुभूति
से समन्वित करने में कितनी सफलता अर्जित की है। इस दृष्टि से कवि विद्यापति ने
ग्राम्य-प्रकृति के अनुकूल चैमासे, बारहमासे की श्रुति मधुर रसधारा भी
प्रवाहित की है। ‘प्रार्थना’ और ‘नचारी’ शीर्षक गीतों में बहुत से गीत ऐसे हैं,
जिनमें सच्चे भक्त की आत्मा का स्वर सुनाई पड़ता है। वार्धक्यमय जीवन
की दीनता, हीनता, विवशता के साथ
समर्पण की अनन्यनिष्ठता की स्वर-सुध की उपलब्धि गायक को साधारण जन जीवन का
प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जब वह कहता है-
कखन
रहब दुख मोर,
हे
भोलानाथ।
दुखहि
जनम भेल, दुखहिं गमाएब,
सुख
सपनहुँ नहीं भेल,
हे
भोलानाथ।।
इस प्रकार यह
स्पष्ट है कि गीतिकार विद्यापति के पद गीतों में निसर्ग जीवन प्रवाह की
मर्मस्पर्शिता है। यौवन और वार्धक्य की सीमा में इनकी कोमल मधुर रागिनी की सरिता
तरल वेग में बहती है। सर्वत्र अनन्यासक्ति में शिशु-सुलभ निश्छलता है। अतएव एक युग
से इनकी स्वरमंदाकिनी सहृदय-हृदय को मुग्ध करती आ रही है।
’’’’’’’’’’’’’’
संदर्भ ग्रंथ:-
1. विद्यापति, सं. डॉ. आनंद प्रकाश दीक्षित, पृ.सं.107, पद सं.13 ।
2. वही, पृ.सं.126, पद
सं.69 ।
3. वही, पृ.सं.125, पद
सं.65 ।
4. वही, पृ.सं.123, पद
सं.58 ।
5. वही, पृ.सं.124, पद
सं.62 ।
6. वही, पृ.सं.127, पद
सं.70 ।
7. वही, पृ.सं.122, पद
सं.57 ।
एसोसिएट
प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, तेजपुर
विश्वविद्यालय, तेजपुर (असम)।


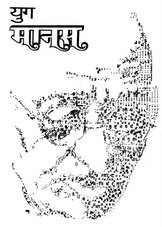
No comments:
Post a Comment