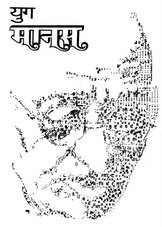आलेख
दीनदयाल उपाध्याय होने का मतलब
पुण्यतिथि पर विशेष (11 फरवरी)
-संजय द्विवेदी
राजनीति में विचारों के लिए सिकुड़ती जगह के बीच पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम एक ज्योतिपुंज की तरह सामने आता है। अब जबकि उनकी विचारों की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली की सत्ता में स्थान पा चुकी है, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय की विचारयात्रा में ऐसा क्या है जो उन्हें उनके विरोधियों के बीच भी आदर का पात्र बनाता है।
दीनदयाल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक पत्रकार, लेखक, संगठनकर्ता, वैचारिक चेतना से लैस एक सजग इतिहासकार, अर्थशास्त्री और भाषाविद् भी थे। उनके चिंतन, मनन और अनुशीलन ने देश को ‘एकात्म मानवदर्शन’ जैसा एक नवीन भारतीय विचार दिया। सही मायने में एकात्म मानवदर्शन का प्रतिपादन कर दीनदयाल जी ने भारत से भारत का परिचय कराने की कोशिश की। विदेशी विचारों से आक्रांत भारतीय राजनीति को उसकी माटी से महक से जुड़ा हुआ विचार देकर उन्होंने एक नया विमर्श खड़ा कर दिया। अपनी प्रखर बौद्धिक चेतना,समर्पण और स्वाध्याय से वे भारतीय जनसंघ को एक वैचारिक और नैतिक आधार देने में सफल रहे। सही मायने में वे गांधी और लोहिया के बाद एक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने भारत को समझा और उसकी समस्याओं के हल तलाशने के लिए सचेतन प्रयास किए। वे अनन्य देशभक्त और भारतीय जनों को दुखों से मुक्त कराने की चेतना से लैस थे, इसीलिए वे कहते हैं-“प्रत्येक भारतवासी हमारे रक्त और मांस का हिस्सा है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगें जब तक हम हर एक को यह आभास न करा दें कि वह भारत माता की संतान है। हम इस धरती मां को सुजला, सुफला, अर्थात फल-फूल, धन-धान्य से परिपूर्ण बनाकर ही रहेंगें।” उनका यह वाक्य बताता है कि वे किस तरह का राजनीतिक आदर्श देश के सामने रख रहे थे। उनकी चिंता के केंद्र में अंतिम व्यक्ति है, शायद इसीलिए वे अंत्योदय के विचार को कार्यरूप देने की चेष्ठा करते नजर आते हैं।
वे भारतीय समाज जीवन के सभी पक्षों का विचार करते हुए देश की कृषि और अर्थव्यवस्था पर सजग दृष्टि रखने वाले राजनेता की तरह सामने आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनकी बारीक नजर थी और वे स्वावलंबन के पक्ष में थे। राजनीतिक दलों के लिए दर्शन और वैचारिक प्रशिक्षण पर उनका जोर था। वे मानते थे कि राजनीतिक दल किसी कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक वैचारिक प्रकल्प की तरह चलने चाहिए। उनकी पुस्तक ‘पोलिटिकल डायरी’में वे लिखते हैं-“ भिन्न-भिन् राजनीतिक पार्टियों के अपने लिए एक दर्शन (सिद्दांत या आदर्श) का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकत्र होने वाले लोगों का समुच्च मात्र नहीं बनना चाहिए। उनका रूप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या ज्वाइंट स्टाक कंपनी से अलग होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि पार्टी का दर्शन केवल पार्टी घोषणापत्र के पृष्ठों तक ही सीमित न रह जाए। सदस्यों को उन्हें समझना चाहिए और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक जुट जाना चाहिए।” उनका यह कथन बताता है कि वे राजनीति को विचारों के साथ जोड़ना चाहते थे। उनके प्रयासों का ही प्रतिफल है कि भारतीय जनसंघ (अब भाजपा) को उन्होंने वैचारिक प्रशिक्षणों से जोड़कर एक विशाल संगठन बना दिया। यह विचार यात्रा दरअसल दीनदयाल जी द्वारा प्रारंभ की गयी थी, जो आज वटवृक्ष के रूप में लहलहा रही है। अपने प्रबोधनों और संकल्पों से उन्होंने तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा जीवनदानी उत्साही नेताओं की एक बड़ी श्रृंखला पूरे देश में खड़ी की।
कार्यकर्ताओं और आम जन के वैचारिक प्रबोधन के लिए उन्होंने पांचजन्य, स्वदेश और राष्ट्रधर्म जैसे प्रकाशनों का प्रारंभ किया। भारतीय विचारों के आधार पर एक ऐसा दल खड़ा किया जो उनके सपनों में रंग भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। वे अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति भी बहुत उदार थे। उनके लिए राष्ट्र प्रथम था। गैरकांग्रेस की अवधारणा को उन्होंने डा.राममनोहर लोहिया के साथ मिलकर साकार किया और देश में कई राज्यों में संविद सरकारें बनीं। भारत-पाक महासंघ बने इस अवधारणा को भी उन्होंने डा. लोहिया के साथ मिलकर एक नया आकाश दिया। विमर्श के लिए बिंदु छोड़े। यह राष्ट्र और समाज सबसे बड़ा है और कोई भी राजनीति इनके हितों से उपर नहीं है। दीनदयाल जी की यह ध्रुव मान्यता थी कि राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते देश के हित नजरंदाज नहीं किए जा सकते। वे जनांदोलनों के पीछे दर्द को समझते थे और समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता की संवेदनशीलता के पक्षधर थे। जनसंघ के प्रति कम्युनिस्टों का दुराग्रह बहुत उजागर रहा है। किंतु दीनदयाल जी कम्युनिस्टों के बारे में बहुत अलग राय रखते हैं। वे जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में 28 दिसंबर,1967 को कहते हैं-“ हमें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो प्रत्येक जनांदोलन के पीछे कम्युनिस्टों का हाथ देखते हैं और उसे दबाने की सलाह देते हैं। जनांदोलन एक बदलती हुयी व्यवस्था के युग में स्वाभाविक और आवश्यक है। वास्तव में वे समाज के जागृति के साधन और उसके द्योतक हैं। हां, यह आवश्यक है कि ये आंदोलन दुस्साहसपूर्ण और हिंसात्मक न हों। प्रत्युत वे हमारी कर्मचेतना को संगठित कर एक भावनात्मक क्रांति का माध्यम बनें। एतदर्थ हमें उनके साथ चलना होगा, उनका नेतृत्व करना होगा। जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं वे इस जागरण से घबराकर निराशा और आतंक का वातावरण बना रहे हैं। ”
इस प्रकार हम देखते हैं कि दीनदयाल जी का पूरा लेखन और जीवन एक राजनेता की बेहतर समझ, उसके भारत बोध को प्रकट करता है। वे सही मायने में एक राजनेता से ज्यादा संवेदनशील मनुष्य हैं। उनमें अपनी माटी और उसके लोगों के प्रति संवेदना कूट-कूट कर भरी हुयी है। ‘सादा जीवन और उच्च विचार’ का मंत्र उनके जीवन में साकार होता नजर आता है। वे अपनी उच्च बौद्धिक चेतना के नाते भारत के सामान्य जनों से लेकर बौद्धिक वर्गों में भी आदर से देखे जाते हैं। एक लेखक के नाते आप दीनदयाल जी को पढ़ें तो अपने विरोधियों के प्रति उनमें कटुता नहीं दिखती। उनकी आलोचना में भी एक संस्कार है, सुझाव है और देशहित का भाव प्रबल है। पुण्यतिथि पर उनके जैसे लोकनायक की याद सत्ता में बैठे लोग करेंगें, शेष समाज भी करेगा। उसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उनके विचारों का अवगाहन किया जाए, उस पर मंथन किया जाए। वे कैसा भारत बनाना चाहते थे? वे किस तरह समाज को दुखों से मुक्त करना चाहते थे? वे कैसी अर्थनीति चाहते थे?
दीनदयाल जी को आयु बहुत कम मिली। जब वे देश के पटल पर अपने विचारों और कार्यों को लेकर सर्वश्रेष्ठ देने की ओर थे, तभी हुयी उनकी हत्या ने इस विचारयात्रा का प्रवाह रोक दिया। वे थोड़ा समय और पाते थे तो शायद एकात्म मानवदर्शन के प्रायोगिक संदर्भों की ओर बढ़ते। वे भारत को जानने वाले नायक थे, इसलिए शायद इस देश की समस्याओं का उसके देशी अंदाज में हल खोजते। आज वे नहीं हैं, किंतु उनके अनुयायी पूर्ण बहुमत से केंद्र की सत्ता में हैं। भाजपा और उसकी सरकार को चाहिए कि वह दीनदयाल जी के विचारों का एक बार फिर से पुर्नपाठ करे। उनकी युगानूकूल व्याख्या करे और अपने विशाल कार्यकर्ता आधार को उनके विचारों की मूलभावना से परिचित कराए। किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता में आना बहुत महत्वपूर्ण होता है, किंतु उससे कठिन होता है अपने विचारों को अमल में लाना। भाजपा और उसकी सरकार को यह अवसर मिला है वह देश के भाग्य में कुछ सकारात्मक जोड़ सके। ऐसे में पं.दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की समझ भी कसौटी पर है। सवाल यह भी है कि क्या दीनदयाल उपाध्याय,कांग्रेस के महात्मा गांधी और समाजवादियों के डा. लोहिया तो नहीं बना दिए जाएंगें?उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता के नए सवार दीनदयाल उपाध्याय को सही संदर्भ में समझकर आचरण करेंगें।
(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं)